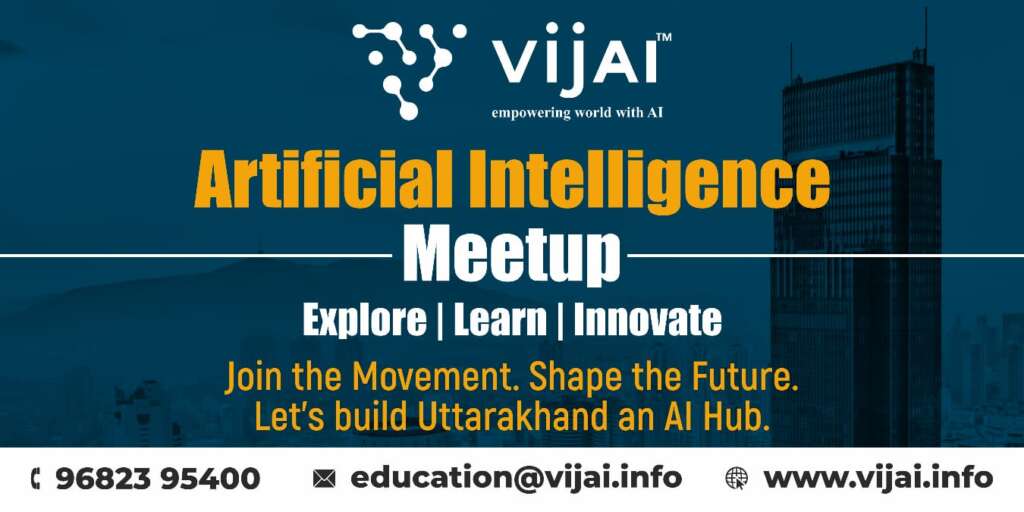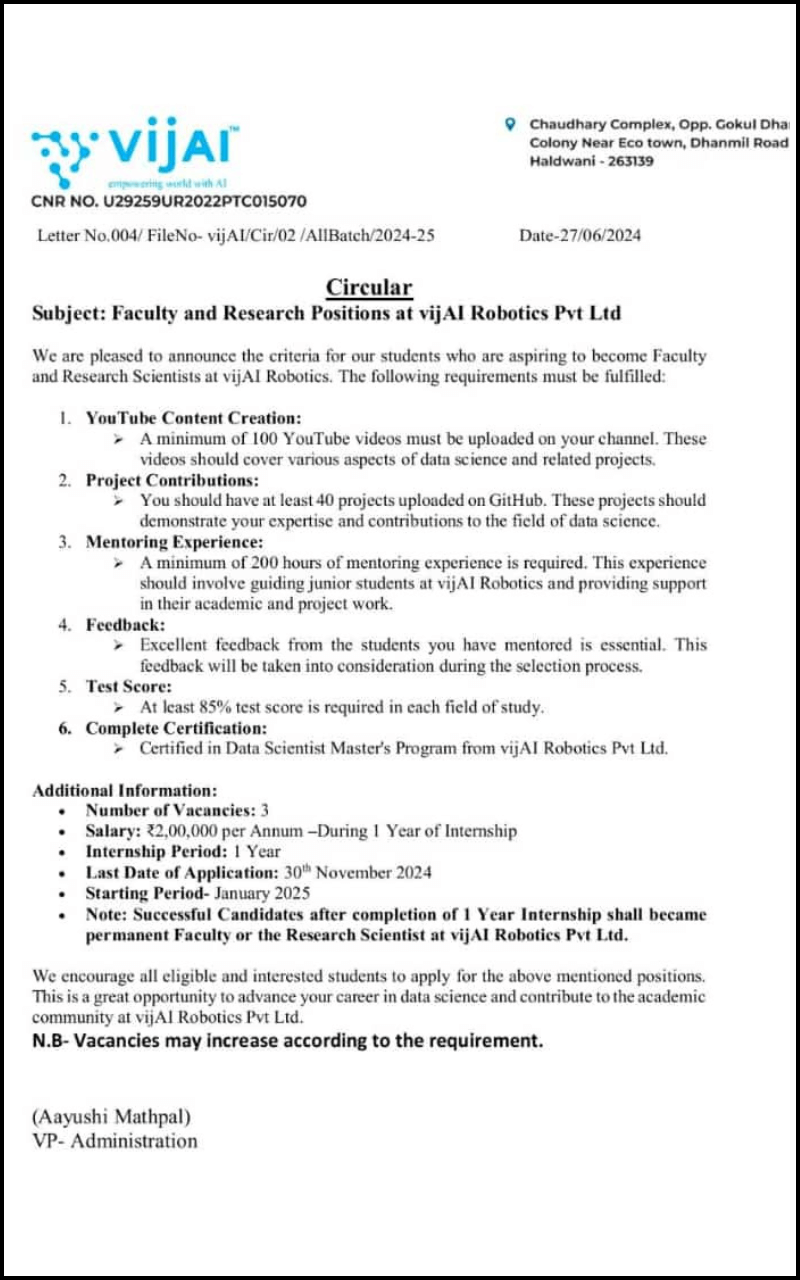श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल का तूफ़ान — भारत के लिए चुनौती, विश्व के लिए सबक।

श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल का तूफ़ान — भारत के लिए चुनौती, विश्व के लिए सबक।
दक्षिण एशिया इस समय गहन राजनीतिक अस्थिरता और जनाक्रोश के दौर से गुजर रहा है। कुछ ही वर्षों में हमारे तीन पड़ोसी देशों — श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शांति पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।
श्रीलंका में 2022 में भयावह आर्थिक संकट ने आम जनता को सड़कों पर ला दिया। ईंधन, दवाइयों और खाद्य आपूर्ति की कमी से जूझती जनता ने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्ज़ा कर लिया, और तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। यह घटना केवल शासन की विफलता नहीं, बल्कि उन संस्थाओं की अस्थिरता का प्रतीक थी जो जनता की आकांक्षाओं को समय पर समझने में असफल रहीं।
इसके बाद बांग्लादेश में पिछले साल बड़े राजनीतिक संकट ने जन्म लिया। विरोधी दलों, कट्टरवादियों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव, चुनावों में पारदर्शिता को लेकर उठते सवाल और जनता की नाराजगी ने हालात को इतना जटिल बना दिया कि लोकतांत्रिक संस्थानों की साख पर गहरा असर पड़ा। पर्दे के पीछे सत्ता के समीकरणों में बदलाव को कई विश्लेषक “शांत तख्तापलट” के रूप में देखते हैं।
अब नेपाल में हाल के हफ्तों में व्यापक जनआंदोलन और हिंसक विरोध ने राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को कठघरे में खड़ा होना पड़ा और प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़ा। यह आंदोलन दर्शाता है कि लोकतांत्रिक सरकारों से जनता की अपेक्षाएँ बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, और आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक असंतोष जब चरम पर पहुँचता है तो बदलाव अवश्यंभावी हो जाता है।
भारत पर संभावित प्रभाव
भारत के लिए ये घटनाएँ केवल पड़ोसी देशों की आंतरिक समस्याएँ नहीं हैं। इनके कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सामने आ सकते हैं:
सीमा-सुरक्षा और शरणार्थी संकट
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल — तीनों की सीमाएँ भारत से सटी हुई हैं। किसी भी राजनीतिक अस्थिरता से शरणार्थियों का पलायन, सीमाई तनाव और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। श्रीलंका संकट के दौरान तमिलनाडु में शरण लेने वाले परिवारों की संख्या इसका उदाहरण है।
आर्थिक और व्यापारिक व्यवधान
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ पहले ही कमजोर हैं। यदि अस्थिरता जारी रहती है तो भारत के निर्यात, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
पड़ोसी देशों का बढ़ता प्रभाव
जब पड़ोसी देशों की सरकारें कमजोर होती हैं, तो बाहरी शक्तियों विशेषकर चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को हस्तक्षेप का अवसर मिलता है। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का उदाहरण बताता है कि आर्थिक दबाव कैसे किसी देश को सामरिक समझौते के लिए मजबूर कर सकता है। भारत के लिए यह भू-राजनीतिक चुनौती और अधिक गंभीर हो सकती है।
क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक संतुलन
भारत को अपनी कूटनीतिक भूमिका को सक्रिय और संतुलित रखना होगा। यदि भारत समय रहते पड़ोसी देशों के साथ संवाद, सहयोग और मानवीय सहायता को प्राथमिकता नहीं देता, तो क्षेत्र में अस्थिरता का दायरा बढ़ सकता है। क्योंकि भारत वैश्विक रूप से अधिक मजबूत देश है।
जनाक्रोश का संदेश और अन्य देशों के लिए सबक
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की घटनाएँ एक स्पष्ट संदेश देती हैं जनता अब शासन की अक्षमता को बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा पीढ़ी, जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म्स से जुड़ी है, पहले से कहीं अधिक जागरूक, संगठित और मुखर हो चुकी है। यदि सरकारें उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझतीं, तो असंतोष बहुत जल्दी व्यापक विरोध का रूप ले सकता है।
इन घटनाओं से अन्य देशों को निम्नलिखित सबक लेने की आवश्यकता है:
आर्थिक स्थिरता सर्वोपरि है :
जब महंगाई, बेरोजगारी और जीवन-यापन की लागत जनता की सहनशक्ति से बाहर हो जाती है, तो राजनीतिक अस्थिरता अनिवार्य हो जाती है। सरकारों को दीर्घकालिक और टिकाऊ आर्थिक नीतियाँ बनानी होंगी।
पारदर्शी और जवाबदेह शासन:
जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होती। उन्हें नीतियों में पारदर्शिता, ईमानदार नेतृत्व और जवाबदेही की अपेक्षा होती है।
युवा वर्ग की भागीदारी :
युवा अब केवल दर्शक नहीं हैं; वे बदलाव के मुख्य वाहक हैं। नीति-निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है।
संवाद और दमन के बीच संतुलन:
कठोर दमन और सेंसरशिप अल्पकालिक समाधान हो सकते हैं, परंतु वे संकट को स्थायी बना देते हैं। संवाद, सहमति और संवैधानिक सुधार अधिक प्रभावी रास्ते हैं।
क्या यह विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी है?
प्रत्यक्ष रूप से ये घटनाएँ वैश्विक युद्ध का कारण नहीं बनतीं, लेकिन क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। अस्थिरता से न केवल व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति-श्रृंखला प्रभावित होती है, बल्कि यह बाहरी शक्तियों के टकराव का मंच भी तैयार कर सकती है। दक्षिण एशिया में बढ़ता तनाव एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, चीन और अन्य शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना सकता है।
निष्कर्ष
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की हाल की घटनाएँ केवल पड़ोसी देशों के आंतरिक संकट नहीं हैं; वे पूरे दक्षिण एशिया के लिए चेतावनी की घंटी हैं। यदि शासन व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ और लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनता की आकांक्षाओं से कट जाती हैं, तो जनआंदोलन और अस्थिरता अपरिहार्य हो जाती है।
भारत के लिए यह समय है कि वह सक्रिय कूटनीति, विकास सहयोग और मानवीय सहायता के माध्यम से पड़ोसी देशों में स्थिरता कायम करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। केवल आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से भी। विश्व के लिए संदेश भी स्पष्ट है जनता की आवाज़ अब पहले से कहीं अधिक प्रबल, संगठित और निर्णायक हो चुकी है। जब तक शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक न्याय पर आधारित नहीं होगा, तब तक विश्व शांति के प्रयास अधूरे रहेंगे।
राजेंद्र कुमार शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार
देहरादून , उत्तराखण्ड।