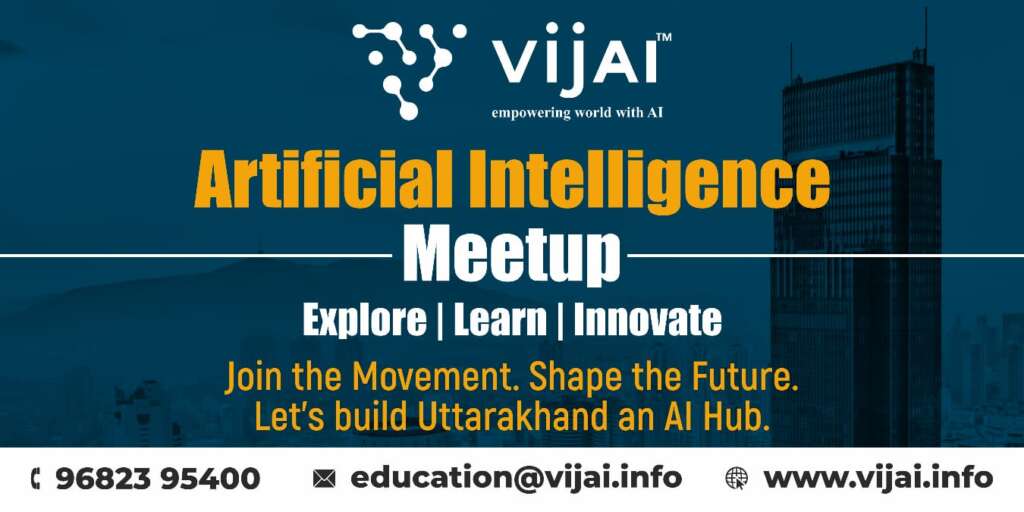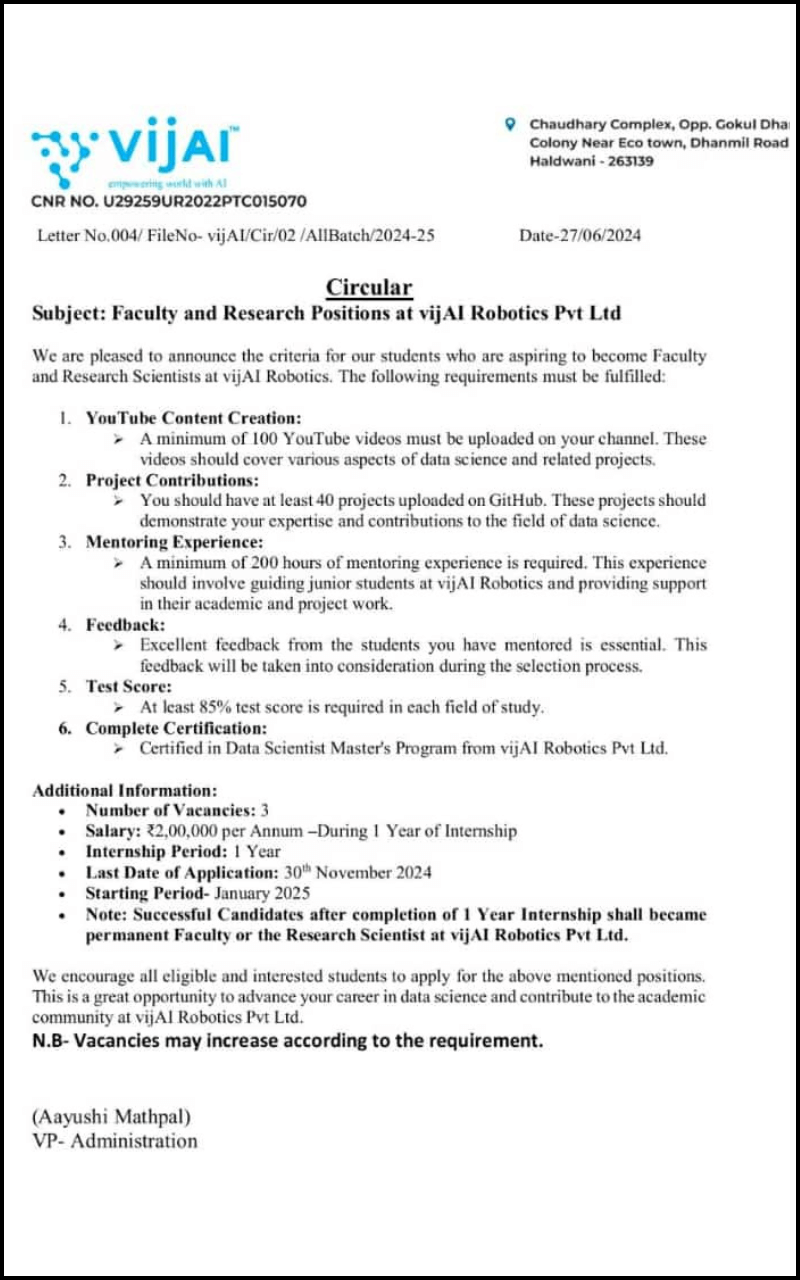उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष पर ठोस रणनीति की आवश्यकता

उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष पर ठोस रणनीति की आवश्यकता
उत्तराखंड इस समय एक ऐसे जटिल मोड़ पर खड़ा है, जहाँ जंगलों की शांति और मनुष्य के जीवन–यापन के बीच की संघर्ष रेखा धीरे–धीरे घनी और गहरी होती जा रही है। पहाड़ों की वह भूमि, जो कभी मानव और वन्यजीव के सहज सह-अस्तित्व की मिसाल मानी जाती थी, आज भय, अविश्वास और अव्यवस्था के एक विचित्र तंत्र में बदल गई है। बीते दस वर्षों में बाघों और गुलदारों की संख्या में आई वृद्धि कागज़ों में वन संरक्षण की सफलता मानी जा सकती है, लेकिन जमीन पर यह स्थिति एक असंतुलित और बिना तैयारी वाली व्यवस्था का दर्पण है, जहाँ वन्यजीवों की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन सुरक्षा, निगरानी और प्रबंधन तंत्र वही का वही जर्जर खड़ा रहा। यह विरोधाभास आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है।
पहाड़ों के गांव पहले ही जनसांख्यिकीय गिरावट की पीड़ा झेल रहे हैं। खाली घरों की लंबी कतारें पहाड़ों के भीतर खड़े उस निर्वासन की गवाही देती हैं, जहाँ जीवन तो है, पर लोग नहीं। वर्षों से बंद पड़े इन घरों के भीतर और आसपास उगी झाड़ियाँ गुलदारों और बाघों के लिए आदर्श निवासस्थल बन चुकी हैं। बंजर घर आज वन्यजीवों के अड्डे बन चुके हैं, और यह अड्डेबाज़ी गांवों के जीवन में भय का स्थायी छाया बनकर उतर आई है। पहाड़ों की संस्कृति में ऐसा कभी नहीं था कि गुलदार घरों की छतों पर घूमते दिखाई दें, लेकिन अब यह सामान्य दृश्य बनता जा रहा है। इस भयावहता के पीछे केवल वन क्षेत्र का विस्तार या संकुचन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह उपेक्षा जिम्मेदार है जो राज्य की नीतियों और प्रशासन की कार्यप्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी है।
इस गंभीर स्थिति के बावजूद राज्य की राजनीति ने इस मुद्दे को समाधान की दृष्टि से अधिक, राजनीति के अवसर के रूप में देखा। बाघ या गुलदार के हमले के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर संवेदना जताना उन नेताओं की प्राथमिकता बन गई है, जिन्होंने वर्षों से वन्यजीव प्रबंधन को कोई नीतिगत महत्व नहीं दिया। कैमरे की चमक में दिखाई देने वाली संवेदनशीलता उस वास्तविक संवेदनहीनता को ढक नहीं पाती, जिसमें न तो दीर्घकालिक रणनीति है, न वैज्ञानिक सोच, न बजट, न जिम्मेदारी। प्रश्न यह है कि विगत तीन वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीव प्रबंधन पर कितना काम किया? कितनी प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम बनाई गई? कितने गांवों में सुरक्षा ढांचा विकसित हुआ? कितने GPS कॉलरिंग की गई? कितने कैमरा ट्रैप लगाए गए? कितने थर्मल ड्रोन खरीदे गए?
इन सवालों के जवाब किसी सरकारी रिकॉर्ड या प्रेस नोट में साफ नहीं मिलते, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन ने वर्षों से समाधान की दिशा में उतनी ऊर्जा नहीं लगाई, जितनी ऊर्जा संवेदना की राजनीति में लगा दी। इसका सबसे बुरा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ा है जो पहाड़ के कठिन भूगोल में रोज़मर्रा की जिंदगी जीते हुए हमेशा इस डर में रहते हैं कि कब कौन सा वन्यजीव उनके रास्ते में आ जाए। उनका दुख अब प्रशासनिक फाइलों की औपचारिकता में बदल चुका है।
वन्यजीव संघर्ष का दूसरा बड़ा प्रश्न पकड़े गए नरभक्षी बाघों और गुलदारों का है। वर्षों से कहा जा रहा है कि अनेक खतरनाक बाघ पकड़े गए हैं, पर ये बाघ गए कहाँ? क्या वे चिड़ियाघरों में सुरक्षित रखे गए? क्या उन्हें किसी रेस्क्यू सेंटर में रखा गया? या फिर फाइलों में स्थानांतरण दिखाकर समाप्त कर दिया गया—जैसे कि एक औपचारिकता पूरी कर दी गई हो? जनता के सामने यह जानकारी कभी पारदर्शिता से नहीं रखी गई। यह अस्पष्टता न केवल प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य में वन्यजीव डेटा और निगरानी कितनी अव्यवस्थित है।
चिड़ियाघरों की स्थिति और भी दयनीय है। न पर्याप्त स्थान है, न आधुनिक बाड़े, न प्रशिक्षित स्टाफ, न वैज्ञानिक उपकरण। ऐसे में किसी भी खतरनाक वन्यजीव को चिड़ियाघर भेजना समाधान नहीं, बल्कि उस समस्या को दूसरे स्थान पर आरोपित कर देना है। जबकि आवश्यकता आधुनिक रेस्क्यू केंद्रों की है, जहाँ वैज्ञानिक निगरानी और सुरक्षित पुनर्वास हो सके।
वन क्षेत्र बढ़ा या घटा, यह भी एक भ्रमित करने वाला प्रश्न है। कागज़ पर वन क्षेत्र बढ़ा दिखाया जा सकता है, क्योंकि उपग्रह हर पेड़ को जंगल मान लेता है, लेकिन जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता—जंगल एक जीवंत पारिस्थितिकी है। सड़क निर्माण, नदी परियोजनाएँ, अवैध कटान, वनाग्नि, अनियंत्रित पर्यटन, चारधाम मार्ग और भू-धंसाव ने जंगलों की गुणवत्ता और निरंतरता दोनों को नुकसान पहुंचाया है। जंगल आज खंड-खंड हो चुके हैं, और खंडित जंगलों में वन्यजीव भोजन और क्षेत्र की तलाश में गांवों की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष की जड़ यही पारिस्थितिक विघटन है, जिसे स्वीकार करने में सरकार हिचकती है।
राजनीतिक इच्छा–शक्ति की कमी को यदि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां सरकारें संवेदनशीलता से अधिक संवेदनशीलता के प्रदर्शन में विश्वास रखती हैं। प्रशासन कम और उद्योगपतियों तथा ठेकेदारों अधिक निर्णय ले रहे हैं। नेता जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व कम और राजनीतिक अवसरों का हिसाब अधिक करते दिखाई देते हैं। यह स्थिति उत्तराखंड को एक ऐसे राज्य में बदल चुकी है, जहाँ राजनीति का उद्देश्य समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि समस्याओं से अवसर पैदा करना बन गया है।
प्रशासन भी इसी तंत्र का एक हिस्सा बन चुका है। परिणाम यह कि उत्तराखंड अपनी समस्याओं का कैदखाना बन गया है। वन्यजीव संघर्ष का एक बड़ा समाधान गांवों में रोशनी की व्यवस्था है। पहाड़ों में रात के समय गांवों के बीच, रास्तों में, खेतों और घरों के आसपास गहरा अंधेरा रहता है। यही अंधेरा गुलदारों की सबसे बड़ी ताकत है। गांव–गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट अनिवार्य होनी चाहिए। यह समाधान न केवल सस्ता है, बल्कि प्रभावी भी। अनेक घटनाओं में यह देखा गया है कि रोशनी वाले क्षेत्र वन्यजीवों की गतिविधि को स्वतः नियंत्रित कर देते हैं।
बंजर और सालों से बंद पड़े घरों के मालिकों को भी कानूनन बाध्य करने की आवश्यकता है। चाहे उन्हें परिसर साफ करवाना पड़े, चाहे घास कटान कराना पड़े, चाहे सुरक्षा दीवार बनानी पड़े। पहाड़ों में ऐसे हजारों घर हैं जो वन्यजीवों के सुरक्षित अड्डे बने हुए हैं। यह घर केवल संरचनाएँ नहीं, बल्कि संघर्ष के बीज बन चुके हैं।
उत्तराखंड को अब भावनाओं से अधिक रणनीति की आवश्यकता है। रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए—जैविक कॉरिडोरों की सुरक्षा, प्रत्येक जिले में त्वरित प्रतिक्रिया टीम, आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति, वैज्ञानिक निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग, वन्यजीव व्यवहार विशेषज्ञों की नियुक्ति, रेस्क्यू सेंटरों का आधुनिकीकरण, ग्राम स्तर पर सुरक्षा समितियाँ और जनजागरूकता कार्यक्रम। सबसे महत्वपूर्ण—राजनीतिक इच्छा–शक्ति और प्रशासनिक जवाबदेही।
उत्तराखंड केवल दृश्यों का प्रदेश नहीं, बल्कि संस्कृति और पारिस्थितिकी का प्रदेश है। यदि यह प्रदेश संघर्ष, भय और कुप्रबंधन का घर बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। राजनीति और प्रशासन को समझना होगा कि पहाड़ की समस्याएँ कैमरों की चमक में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और दृढ़ निश्चय में छिपी हैं।
आज पहाड़ पुकार रहा है—
हमें संवेदना नहीं, समाधान चाहिए।
हमें राजनीति नहीं, सुरक्षा चाहिए।
हमें भाषण नहीं, प्रबंधन चाहिए।
हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, दिखावटी सरकार नहीं।
यही पहाड़ की आवाज़ है, यही जनता की मांग है, और यही समय का निर्णायक संदेश—
उत्तराखंड को अब दिखावे की नहीं, ठोस रणनीति की आवश्यकता है।
डॉ. किशोर कुमार पंत, लेखक एवं सोशल, एक्टिविस्ट